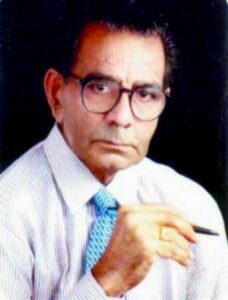 रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।
रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।त्रयोदशोऽध्यायः – ‘क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग’
अध्याय तेरह – ‘शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज है, और इन दोनों में अन्तर’
श्लोक (२१)
त्रिगुणात्मक रही प्रकृति अर्जुन, जीवात्मा जिसमें वास करे
जो कर्म करे जो इच्छायें, वैसी ही उसको योनि मिले
वह भोग भोगता अपना ही, अपने कर्मो का फल पाता
उत्तम या अधम योनियों का, वह ही होता है निर्माता
आत्मा जो प्रकृतिवास करती, उपभोग गुणों का करती है,
गुण में आसक्ति रही जैसी, वैसा भविष्य वह गढ़ती है।
अच्छे या बुरे कर्म जैसे, वे करें योनि का निर्धारण,
जीवात्मा मुक्त न हो पाती, वह करे जन्म पुनि पुनि धारण ।
सात्विक गुण के जो कर्म रहे, सत्कर्म उठाते हैं ऊँचा,
मध्यम हैं कर्म रजोगुण के, यह पलड़ा उठता या गिरता ।
जो कर्म तभी गुण के निषिद्ध, वे पतित रहे वे करें पतन,
सुख भोगा करता सत्कर्मी, दुख भोगा करता पतित गहन ।
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, जीवात्मा जिनमें वास करे,
उसका सम्बंध प्रकृति से है, वह प्राकृत गुण का भोग करे।
भोक्तापन ही जीवात्मा को, बांधे रखता है बन्धन में,
वह कभी मुदित उल्लसित दिखे, या कभी विलपता क्रन्दन में।
वह पाए ऊँची योनि कभी, या नीची योनि कभी पाता,
जैसी उसकी आसक्ति रही, जैसी संगति वह अपनाता ।
जैसा बन जाता संस्कार, वैसा ही बुद्धि काम करती,
सुधि अंत समय में जब आती, जीवात्मा मुक्तिलाभ करती ।
यह प्रकृति रही गुणमयी पार्थ, करती रहती कौतुक अनेक,
यह क्षण प्रति क्षण है, चिरनूतन, यह सक्रिय अपने गुण समेत ।
यह जड़ पदार्थ से भी अपने, करवा लेती है, सभी काम
जग-जीवन में इसके कारण, पाते प्रसिद्धि कितने न नाम?
हो गया प्रेम से युक्त नेह, इन्द्रियाँ दक्ष चैतन्य हुई,
मन तीनों लोकों में घूमा, फिर भी न वासना तृप्त हुई ।
रचती यह भ्रम का वृहत द्वीप, यह स्वयं रही आमूर्त व्याधि
यह मूर्ति अमर्यादा की है, मायाविनि है इसकी उपाधि ।
अनगिनत किये पैदा विकार, यह काम रुप वल्लरि बढ़ती,
बँक लेती फूलों पत्तों से, जिस मण्डप के ऊपर चढ़ती ।
यह मोह विपिन की रितु बसन्त, है अन्तहीन इसकी माया,
यह निराकार को आकृति दे, जग का प्रपंच इसका साधा ।
विधाएँ सभी, कलाएँ सब, उत्पन्न हुआ करती इससे,
इच्छा की, ज्ञान, क्रियायों की, उत्पत्ति हुआ करती इससे ।
टकसाल नाद के सिक्के की, यह चमत्कार का रही सदन,
इसका ही सारा खेल रहा, हो जग-जीवन या प्रलय मरन ।
उत्त्पत्ति और लय, भोर-साँझ, इसका अद्भुत है इन्द्रजाल,
सहचरी पुरुष की यह अभिन्न, जो है असंग, जो निराकार ।
सामर्थ्य रहा इसका विस्तृत, यह पुरुष पुरातन को साधे,
यों इसमें कुछ सविशेष नहीं, यह रुप किसी का भी धारे
उत्पत्ति बने यह ब्राह्म की, उस निराकार को आकृति दे,
इच्छा विहीन की इच्छा बन, उस निश्चल को अपनी गति दे ।
जो पूर्ण उसे दे तृप्ति तोष, उस अकुल, विरज की बने जाति,
लक्षण बन रहे अवर्णन का, निर्जर की वह बन रहे पाँति
वह निरहंकार का अहंकार, वह नाम रहित का बने नाम,
वह जन्म रहित का जन्म बने, वह क्रियाहीन का बने काम ।
निर्गुण के गुण वह बन जाती, वह उस अनेत्र के नेत्र बने,
वह श्रवण रहित के बने कान, वह निस्सीमित का क्षेत्र बने ।
जो भावातीत भाव उसका, अवयव उसका जो निरावयव,
जिसका न अंत, वह अंत बने, जिसका न आदि, उसका उद्भव ।
सब कुछ बन सकती है माया, उस ब्रह्म रुप पुरुषोत्तम का,
माया की माया का विकार, अविकारी में दीखे भरता ।
हो जाता तेज लुप्त शशि का, जिस तरह अमावस आने पर,
ब्रह्म का तेज न दिख पाता, तम, प्रकृति-भाव का छाने पर ।
बादल आकर दोपहरी में, जिस तरह तेज रवि का हरते,
हो पुरुष अधीन प्रकृति के तो, पट, कान्तिहीन उसको करते।
गुण-भोग भोगना पड़ता है, सुख-दुख का होता है अनुभव,
निर्गुण पर छाया दिखता है, झूठा यह जन्म-मरण का भव ।
चल जल में बिम्ब अनेक बनें, शशि मूल रुप में एक रहे,
है पुरुष एक पर माया में, जग उसके विविध प्रकार लखे । क्रमशः….