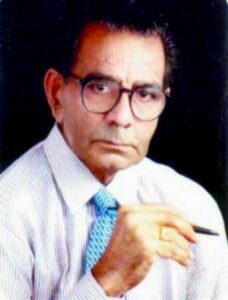 रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।
रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।नवमो ऽध्यायः – ‘राज गुहययोग’
अध्याय नौ – ‘राजविद्या राजमुख्य योग’ सबसे बड़ा ज्ञान/रहस्य, ‘भगवान अपनी सष्टि से बड़ा है’
श्लोक (18)
मैं गति जो पाने योग्य रही, मैं हूँ सबका पालनकर्ता,
मैं घट-घट वासी परमेश्वर, मैं रहा शुभाशुभ का दृष्टा ।
मैं परमधाम, अशरण-शरण, मैं अन्तरंग सबका साथी,
मैं सृष्टि प्रलय विश्रामस्थल, आधारबीज मैं अविनाशी ।
मैं ठाँव जहाँ विश्राम करे थक चुकी प्रकृति प्रलयान्तर पर,
फिर बस जाता है विश्व नया, जिससे नव जीवन धारण कर ।
मैं लक्ष्मीपति, मैं स्वामी हूँ, त्रिभुवन का दस दिक्पालों का,
जिसको जैसी आज्ञा मिलती, वह आज्ञा का पालन करता ।
आकाश रहे सर्वत्र व्याप्त, क्षण भर भी शान्त न वायु रहे,
नित जले आग, घनवृष्टि करे, पर्वत न जगह से कहीं हिले ।
मर्यादा तोड़े नहीं सिन्धु, सहचले भार पृथ्वी जग का,
जिसका जो कर्म रहा उसको, हर एक सजग रहकर करता ।
मेरे कहने से चले सूर्य, कहने से बोलें वेद सभी,
मेरी गति से गतिवान प्राण, जीवन पाते हैं जीव सभी ।
भूतों को ग्रसताकाल बली, पालन कर मेरी आज्ञा का,
सारा जग मेरे शासन में, मैं नाथ रहा सारे जग का ।
उत्पन्न नीर से लहर हुई, लहरों में भी ज्यों नीर रहे,
त्यों जग में मैं रहता अर्जुन, मुझमें सारा संसार रहे ।
गह लेता मेरी शरण उसे मैं जन्म मृत्यु से मुक्त रखें,
शारणागत का मैं हूँ रक्षक, अपने भक्तों का कवच बनूँ।
जो ब्रह्मदेव से मच्छर तक, प्रिय रहा सभी को वह मैं हूँ,
जीवन हूँ तीनों भुवनों का, उतपति, लय का कारण मैं हूँ।
मेरे कारण फूटा करती हैं, वृक्ष-वृक्ष में शाखायें,
वे वृक्ष बीज में मेरे ही हो पुंजीभूत समा जायें ।
आकार व्यक्त सब हो विनष्ट, मुझमें ज्यों बिन्दु समा जाता,
मुझ निराकार में लीन जगत, फिर नहीं दृष्टिगत हो पाता ।
जितने भी रुप विधान रहे, मुझमें विलीन सब हो जाते,
बचता न वर्ण, बचता न भेद, सब गहन नींद में खो जाते ।
मैं उन्हें सुलाने वाला हूँ, मैं ही हूँ उनकी नींद गहन,
मैं किए रहूँ उनको धारण, जब तक हो जाता नहीं सृजन ।
करता हूँ जब उत्पन्न ताप, नभ मण्डल का सूरज बनकर,
जल जलकर बनता वाष्प, बनाया करता मैं जिसको जलधर
श्लोक (१९)
हे अर्जुन सूर्यरुप मैं ही, तपता हूँ, जग को तपा रहा,
मैं सुखा रहा जल पृथ्वी से, मैं बादल बनकर झरा रहा ।
मैं अमृत मूर्तिमान दुर्लभ, मैं कालकूट हूँ मृत्यु रुप,
मैं सत का रहा अभाव असत, मैं सत की व्यापक विमल धूप ।
करता हूँ जब उत्पन्न ताप, नभ मण्डल का सूरज बनकर,
जल जलकर बनता वाष्प, बनाया करता मैं जिसको जलधर ।
जब अग्नि जलाती लकड़ी को, लकड़ी हो जाती अग्नि रुप,
जो मार रहा, जो मरता है, ये दोनों मेरे रहे रुप ।
जो गए मृत्यु के मुख में वे, मानों मेरे उदरस्थ हुए,
मुझ अविनाशी से ही अर्जुन, सत और असत ये जग प्रगटे ।
क्या ऐसी कोई जगह कहीं, मैं जहाँ न होऊँ विद्यमान ?
वे आंखों के अन्धे होते, चाहा करते हैं जो प्रमाण ।
संसार रहा मदरुप पार्थ, फिर भी न मुझे वह पहिचाने,
आड़े आते हैं कर्म कि वह, मुझमें रहकर न मुझे जाने ।
रहता न ज्ञान जिनको यथार्थ, वे बिना पंख के गरुड़ रहे,
सत्कर्म रहे जो जीवन के, वे बिना ज्ञान के नहीं फले ।
कोई भी रुप भजे प्रभु का, पर वह जो पूजा करता है,
स्वीकार प्रार्थनाएँ होती, वह पात्र कृपा का बनता है ।
सत असत सुधा या काल रुप, प्रभु की पहिचान हुई जिसको,
– कर्मों को सार्थक कर लेता, मिल जाता उचित मार्ग उसको । क्रमशः….