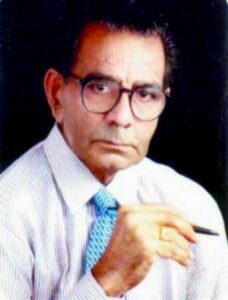 रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।
रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।नवमो ऽध्यायः – ‘राज गुहययोग’
अध्याय नौ – ‘राजविद्या राजमुख्य योग’ सबसे बड़ा ज्ञान/रहस्य, ‘भगवान अपनी सष्टि से बड़ा है’
श्लोक (१५)
होते हैं अन्य ज्ञान योगी, मुझ निराकार का करें यजन,
साधें वे ज्ञान यज्ञ अपना, मदरुप हुए करते पूजन ।
उनसे भी भिन्न मनुष्य रहे, जो विविध रुप से पूज रहे,
उनकी पूजा के कारण ही, जग में मेरे बहुरुप रहे ।
मैं एक विराट पुरुष लेकिन, लोगों की आस्था भिन्न रही,
उनकी उपासना पृथक रही, गढ़ती जो मेरे रुप कई ।
यह रही उपासना मेरी ही, सब देव रुप मेरे अर्जुन,
आराधन उनका सफल करूँ, स्वीकार मुझे उनका पूजन ।
हो चन्द्रसूर्य या अग्नि वरुण, या देवों के पति इन्द्रदेव,
मेरे ही अंश रहे अर्जुन, सबका स्वामी मैं एकमेव ।
जिसकी भी पूजा जग करता, करता है वह मेरी पूजा,
फलदायक इष्ट रहा उसको, वह इष्ट नहीं कोई दूजा
अतिरिक्त भक्ति के ऐसे भी, जो कर ज्ञान का अनुशीलन,
वे मुझे कि मुक्त परमेश्वर को, अपने ढंग से भजते अर्जुन ।
कोई भजते मुझ अद्वय को, कोई भजता बहुरुपों में,
कोई उपासता विश्वरुप, भजते जन विविध स्वरुपों में ।
मैं रहा किसी को ज्ञान यज्ञ, मैं रहा किसी को विधि रुप,
हर एक दिशा अभिमुखी रहा, मैं रहा किसी को एक रुप ।
जैसा जिसने देखा मुझको, वैसी करता मेरी पूजा,
मैं एक रुप अस्तित्वों में, मैं पृथक रहा उनसे दूजा ।
रे ब्रह्मदेव से लघु तृन तक, सब में आत्मा है भरी हुई,
मिट जाता जीवभाव उसका, आत्मा जिसकी हो जगी हुई ।
इस तरह ज्ञान से एक रुप, जग में करते मेरा दर्शन,
नाना रुपों में जगत रहा, पर भेद न करते वे अर्जुन ।
यह भेद अवयवों का केवल, लेकिन शरीर में भेद नहीं,
शाखायें हो लघु दीर्घ भले, लेकिन होता है पेड़ वही ।
अनगिनती किरणें सूरज की, पर सूरज तो बस एक रहा,
नानाविध भूतों के भीतर जो आत्मतत्व वह एक रहा ।
इस तरह जानते जो मुझको, जो ज्ञान यज्ञ साधा करते,
जो भीतर है, वह ही बाहर, वे भेद न कुछ माना करते ।
सर्वत्र वायु से भरा हुआ, आकाश नहीं खाली कोना,
हो गया ब्रह्म का ज्ञान जिसे, तय उसका मुझमें लय होना ।
श्लोक (१६)
क्रतु याने श्रौतकर्म हूँ मैं, मैं यज्ञ कि हूँ स्मार्त-कर्म,
मैं क्रिया पितृतर्पण की हूँ, मैं रोग विनाशक जड़ी धर्म ।
मैं मन्त्रजाप, ध्वनि हूँ चिन्मय, मैं अग्नि होमघृत हवन क्रिया,
जो भावित रहा भावना में, उसकी सार्थक प्रत्येक क्रिया
मैं उदयज्ञान का रहा वेद, मैं वेद विहित हूँ अनुष्ठान,
मैं ऋतु से जो उत्पन्न कर्म, मैं रहा यज्ञ मैं कर्मकाण्ड ।
मैं ही देवों का आराधन, मैं ही पितरों का पिण्डदान,
मैं औषधि हूँ, मैं मन्त्र रहा, मैं घृत हूँ, मैं ही कृशान ।
संपूर्ण प्रकृति की आहुति का आवाहन करता यज्ञ कर्म,
दर्शाता भाव समर्पण का, विश्वात्मा के प्रति विहित धर्म ।
हम जो कुछ प्रभु से लेते हैं, उसको ही सब लौटा देते,
उपहार उसे उसके देकर हम ऊऋण उससे हो लेते ।
देवों पितरों को खुश करने, मानव जो कर्म किया करता,
सम्पन्न ‘यज्ञ’ को करने में, जो कारक या कारण बनता
वह सब मैं ही हूँ, भेद न कर, मैं साध्य स्वयं बनता साधन,
मैं यज्ञ, स्वधा, मैं हवन, हव्य, मैं मन्त्र जाप, मैं आवाहन ।
श्लोक (१७)
मैं हूँ इस जग का जगत पिता, मैं सारे जग की माता हूँ,
मैं पालक हूँ, मैं पोषक हूँ, मैं सबका भाग्य-विधाता हूँ।
मैं ज्ञेय परम ओंकार दिव्य, मैं शब्द ब्रह्म ऋग्वेद रहा,
मैं सामवेद संगीत मधुर, मैं यजुर्वेद धनु-तीर रहा
अष्टाग प्रकृति उत्पन्न कर जग को जिससे कर आलिंगन,
वह अर्द्ध नटेश्वर मैं ही हूँ, वह जगत्पिता मैं ही अर्जुन ।
जड़ जंगम की मैं ही माता, वह धरती जिस पर जगत बसे,
जो पाले-पोसे अग जग को, वह धाता मैं जो विश्व रचे ।
अर्जुन मैं त्रिभुवन का आजा,रे प्रकृति-पुरुष का पिता रहा,
वेदों का हूँ वह ज्ञान जहाँ एकात्म समत्व भाव उभरा ।
सिद्धांत सभी हो एक रुप, भ्रम को कर दूर पवित्र हुए,
ओंकार प्रणव के अक्षर से, ऋक यजुर्साम आगम प्रगटे । क्रमशः…