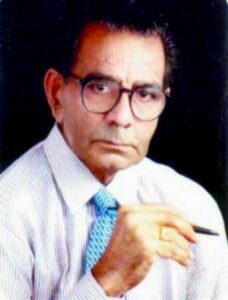 रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।
रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।पञ्चदशोऽध्यायः – “पुरुषोत्तम योग’ अध्याय पंद्रह – ‘जीवन का वृक्ष’
क्षर पुरुष (क्षेत्र), अक्षर पुरुष (क्षेत्रज्ञ), और पुरुषोत्तम (परमेश्वर)- तीनों का वर्णन, क्षर और अक्षर से भगवान किस प्रकार उत्तम हैं, किसलिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आदि- पुरुषोत्तम योग,
श्लोक (१३)
करके प्रवेश सब लोकों में, मैं ही उनको धारण करता,
लोकों के सारे जीवों का, जीवन समस्त मुझसे चलता ।
तरु पौधे सभी वनस्पतियाँ, मेरे द्वारा सीचीं जातीं,
मैं रहा चन्द्रमा अमृतमय, मुझसे ही वे पोषण पातीं ।
मैं पृथ्वी में होकर प्रविष्ट, करता हूँ उसका भार वहन,
बन प्राण प्राणियों का, उनको, अवनीतल पर करता धारण।
सब जड़ी-बूटियाँ सींच रहा, मैं सोम, सुधा रस बरसाकर,
पालन-पोषण करता जग का, फल फूल रहा जग हरयाकर ।
सब भूतों को धारण करता, पृथ्वी का भार उठाकर मैं,
औषधियों को परिपुष्ट करूँ, शशि बन, अमृत बरसाकर मैं।
मेरे ही हैं ये अंश सभी, जारज, पिण्डज, उदभिज सारे,
पोषण धान्यों का करता मैं, रक्षित मुझसे प्राणी सारे ।
श्लोक (१४)
मैं अनल वैशवानर बनकर, हूँ अग्नि उदरगत प्राणी की,
जो भक्ष्य, भोज्य अरु चोष्य लेह, भोजन का नित पाचन करती।
मैं प्राणवायु में वैसा ही, जैसा अपान में बसता हूँ,
उत्पन्न न केवल अन्न करूँ, मैं पचा उसे रस बनता हूँ।
मैं प्राणिमात्र की देहों में, जीवन की अग्नि बना रहता,
प्राणों को रखूँ नियन्त्रित मैं, सारे आघातों को सहता ।
भोजन का करता हूँ पाचन, रस से तन को बलवान करूँ,
नव शक्ति प्रदान करूँ सबको, जीवन क्रम को गतिमान रखूँ ।
मैं ही वैशवानरअग्नि रुप, प्राणों से मैं जुड़कर रहता,
पाचन करता हूँ भोजन का, जिससे जीवन का रस बनता ।
खायें, निगलें, चाटें, चूसें, उदरस्थ धान्य को पचना है,
बनना है उससे जीवन-रस अर्जुन यह मेरी रचना है ।
प्राणि मात्र के नाभिकन्द की, भट्टी को मैं ही सुलगाता,
प्राण अपान वायु के द्वारा, मैं उसमें जठराग्नि जगाता ।
तरह-तरह के अन्न सभी का, करता रहता मैं ही पाचन,
मैं ही जीव, जगत मैं ही हूँ, मैं ही सबका भोजन अर्जुन ।
मुझसे भरा हुआ जग सारा, बुद्धि तत्व आभास कराये,
शुद्ध बुद्धि में अंकित हो छवि, दूषित में भ्रम बढ़ता जाये ।
स्वाति बूँद सीपी में मोती, वही गरल अहि के मुँह पड़कर,
एक मुक्त रहता जीवन में, फँसे एक माया में पड़कर ।
पानी एक, भेद बीजों का, अलग-अलग तरु-दल उपजाये,
बुद्धि भेद से विविध रुप में यह स्वरुप मेरा बंट जाये ।
होता सूर्योदय कितने ही, जग-व्यवहार शुरु हो जाते,
ज्ञानी सुख का संचय करता, अज्ञानी दुख रहे बढ़ाते ।
हो शक्ति प्रकाशन की चाहे, या शक्ति धारणा की अर्जुन,
पोषण की शक्ति रहे चाहे, या शक्ति कि जो करती पाचन ।
ये सभी शक्तियाँ मेरी ही, मेरे अंशों से काम करें,
जितने भी कार्य कलाप रहे, मेरा आश्रय पाकर विकसें । क्रमशः…