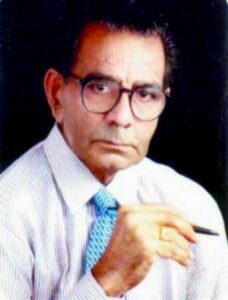 रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।
रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।त्रयोदशोऽध्यायः – ‘क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग’
अध्याय तेरह – ‘शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज है, और इन दोनों में अन्तर’
श्लोक (1)
श्री भगवानुवाच:-
केशव बोले कौन्तेय सुनो, जो पुञ्ज इन्द्रियों का शरीर,
कहते हैं क्षेत्र इसे अर्जुन, जिसमें रहता है बद्ध जीव ।
यह कार्य क्षेत्र जीवात्मा का, जिसने इस सच को पहिचाना,
कहलाता है क्षेत्रज्ञ वही, तन क्षेत्र तथ्य जिसने जाना ।
तन को कहते हैं क्षेत्र पार्थ, इसका ज्ञाता ‘क्षेत्रज्ञ’ रहा,
ज्ञानी जन ऐसा बतलाते, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जान रहा ।
आत्मा देखे जाने जिसको, जिसमें बसता है यह शरीर,
आत्मा के लिए शरीर क्षेत्र, ‘क्षेत्रज्ञ’ किए धारण शरीर ।
आत्मा क्षेत्रज्ञ, शरीर क्षेत्र, आत्मा जाने, देखे तन को,
तन दृश्य रुप, दृष्टा आत्मा, क्षय होता क्षेत्र कहें जिसको ।
यह क्षेत्र कि खेत समान रहा, अंकुराते पाकर समय बीज,
कर्मो के फल फलते जिसमें, यह क्षेत्र विलक्षण रहा चीज ।
तत्वज्ञ महात्माजन कहते, जिसका क्षय हो, वह क्षेत्र रहा,
तन नाशवान इस कारण ही, क्षय पुरुष इसे है कहा गया ।
यह तथ्य जानता जो ज्ञानी, क्षेत्रज्ञ रहा द्रष्टा आत्मा,
वह चेतन परम विलक्षण है, अधिपति शरीर का है आत्मा ।
क्षेत्रज्ञ क्षेत्र में बसता है, वह ज्ञाता चेतन तत्व रहा,
वह अविनाशी, वह शाश्वत है, वह नित्य अलिंग, अविकार रहा।
जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन्हें, इनके स्वरुप में जान रहे,
वे रहे तत्ववेत्ता अर्जुन, गुण-धर्म विलक्षण धार रहे ।
हे अर्जुन यह शरीर क्षेत्र, वह मनुज जानता जो इसको,
जो तत्व जानने वाले हैं, क्षेत्रज्ञ कहा करते उसको ।
या कहो देह यह क्षेत्र रही, जो होता है इसका ज्ञाता,
जाने जो क्षेत्र किसे कहते, उसको ‘क्षेत्रज्ञ’ कहा जाता
यह क्षेत्र शरीर रहा जिसमें, घटती रहती हैं घटनाएँ,
आता बचपन, यौवन आता, फिर जरा, छूट फिर सब जाएँ।
बढ़ना घटना फिर मृत्युपाश, सब इसी क्षेत्र में हैं घटते,
चेतन रह अनासक्त निष्क्रिय, क्षेत्रज्ञ रहे यह सब लखते ।
सक्रिय है प्रकृति अचेतन यह, निष्क्रिय है पुरुष चेतना रे,
चेतन में और पदार्थों में, यह रहा सुपरिचित अन्तर रे ।
है साक्षी भाव जहाँ केवल, वह रहा चेतना का निवास,
जड़ प्रकृति रही निष्क्रिय लेकिन, उसमें गतिविधि का है विकास।
क्षेत्रज्ञ, चेतना का प्रकाश, यह सभी पदार्थो को जाने,
यह तनधारी मन नहीं मात्र, अग जग को एक विषय माने ।
सारा ब्रह्माण्ड पदार्थ रहा, उस महाचेतना के आगे,
जिसको न इन्द्रियाँ या मन की, आवश्यकता कोई जागे ।
क्षेत्रज्ञ पार्थ परमेश्वर है, जो जग का विषय न वस्तु रहा,
सब क्षेत्रों का वह ब्रह्मा है, सबमें होकर भी पृथक रहा ।
उसकी न रही कोई सीमा, उसकी कोई श्रेणी न रही,
वाणी परिभाषित कर पाए, गूँथी कोई वेणी न रही ।
क्षेत्रज्ञ रुप जो मनुज रहा, वह दुहरा आत्मविरोधी है,
वह मुक्त रहा, व बन्धा रहा, वह प्रकृति-पुरुष संयोगी है।
जड़ प्रकृति रही उसका शरीर, अरु जीवात्मा है पुरुष-प्राण,
देवत्व प्राप्त करना चाहे, पतनोन्मुख भी उसका प्रयाण
मानो अवतीर्ण प्रकृति में वह, उसका निर्धारण प्रकृति करे,
भय, चिन्ता, इन्द्रिय वेगों को, धारण कर प्राणी पतित बने।
लेकिन वह पतित प्रकृति पर भी, पाने को विजय प्रयास करे,
वह नहीं प्रकृति के आश्रित शिशु, वह अपना कर्ता आप बने ।
वह तात्विक प्रकृति शक्तियों से, प्रेरित भावित होता लगता,
लेकिन अदम्य इच्छा लेकर, वह प्रकृति जीत लेने बढ़ता ।
कर्ता बन जाता कर्मों का, वह पुरुष बने, क्षेत्रज्ञ बने,
वह द्रव्य पदार्थ नहीं रहता, अस्तित्ववान वह ब्यष्टि बने ।
करता असीमता में प्रवेश, उसमें असीमता सिमट बसे,
क्षेत्रज्ञ रुप ऐसा पाता, जिसकी कोई समता न रहे ।
आवृत्ति नहीं उसकी होती, वह परम विशिष्ट अकेला है,
वह एक अकेला है लेकिन, उसमें समष्टि का मेला है ।
वह सार्व भौम हो जाता है, सविशिष्ट इकाई बन रहता,
मानव-प्राणी संयोग गूढ़, जो एक अनेक साथ रहता ।
वह नहीं पूर्ण का अंश मात्र, वह स्वयं रहा सम्भाव्य पूर्ण,
पूर्णत्व प्राप्ति के लिए सजग, करता अपने संकल्प पूर्ण ।
हर अन्तर्वस्तु सार्वभौमिक, उसके अन्तस में बसती है,
उपलब्ध पूर्णता को करने, उसकी हर साध उमगती है ।
एकत्व पूर्णता है उसकी, जिसको वह पा ही जाता है,
वह मूल आन्तरिक तत्व साध, जीवन सार्थक कर लाता है।
दा आख या दा हाथा म, मानव की नहीं विलक्षणता,
वह उसके अन्तस में बसती, जिसमें है मूल तत्व बसता ।
वह तत्व सृजन का कारण बन, गुणमय कर देता जगत सकल,
भय की बाधा को हर लेता, उसके संग चले मरण का दल ।
यह अद्भुत है उसकी क्षमता, सामान्य नहीं होती विशिष्ट,
व्यक्तित्व निराला गढ़ती है, होकर असीमता में प्रविष्ट ।
व्यक्तित्व रहे बेजोड़ मुक्त, दुहराया उसे न जा सकता,
उसके बदले में नहीं दूसरा, उस जैसा लाया जा सकता ।
बनता ऐसा वह रुपवान, जिसकी समानता नहीं मिले,
वह बिल्कुल नई निराली छवि, के साथ जगत के बीच खिले ।
मंजिल पर उसे पहुंचना है, पाना होता अपना स्वरुप,
वह सूरज बनकर स्वयं जिए, या सूरज की बन रहे धूप । क्रमशः….