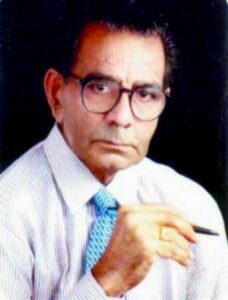 रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।
रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।द्वादशोऽध्यायः – ‘भक्तियोग’
‘व्यक्तिक भगवान की पूजा, परमब्रह्म की उपासना की अपेक्षा अधिक अच्छी है’
श्लोक (१६)
स्पृहा रहित जिसके मन में, रहती न अपेक्षा प्रतिफल की,
जो हो पवित्र बाहर भीतर, हो व्याप्ति नहीं जिसको दुख की ।
जो कुशल रहा, आसक्ति रहित, जो अनासक्त, जो उदासीन,
वह फलासक्ति से रहित भक्त, मुझको अति प्रिय वह जन प्रवीण ।
आकांक्षा से रहित पुरुष जो अन्तर-बाह्य विशुद्ध रहा,
पक्षपात से रहित रहा जो, ज्ञान प्राप्ति में दक्ष रहा ।
प्रभु इच्छा को अपनी इच्छा, समझ आचरण जो करता,
सब आरम्भवों का त्यागी वह, भक्त मुझे अति प्रिय लगता ।
रखता न किसी से कुछ आशा, जो कर्मकुशल, मन से पावन,
निरपेक्ष, निराग्रह, कष्ट रहित, चुन लेता जो पथ मनभावन ।
झूठे सपनों में उड़े नहीं, क्या कर्म, उसे करना जाने,
जग में करणीय मार्ग चुनता, उस पर सधकर चलना जाने ।
कर्मों के फल का त्याग किए, जो कार्य कुशलता से करता,
जो दक्ष, शुद्ध, वासना रहित, अपने पथ को प्रशस्थ करता ।
दुःख द्वेष रहित, रहता प्रसन्न, इच्छा न करे सरबस त्यागी,
करता है मेरी भक्ति पार्थ, मैं रहा भक्त का अनुरागी ।
श्लोक (१७)
जो कभी नहीं हर्षित होता, करता है जो विद्वेष नहीं,
जो शोक न करता कभी पार्थ, मन में न कामना रही कहीं।
शुभ अशुभ कर्म के फल जिसने, संपूर्ण रुप से त्याग दिए,
वह मेरा भक्त मुझे है प्रिय, जो हो असंग, मम साथ जिए।
नहीं कामना करता कोई, मन में विरति जगाता है,
हर्षित होता नहीं, न करता द्वेष, न शोक मनाता है ।
अच्छे बुरे सभी कर्मो का, रहता जो सच्चा त्यागी,
भक्ति युक्त वह पुरुष मुझे अतिप्रिय रहता जो अविकारी ।
आत्म रुप से बढ़कर जिसको, कोई वस्तु न भाती है,
पाकर आत्म स्वरुप न उसको, चाह शेष रह जाती है ।
सूरज को क्या भेद रात या दिन, का कुछ भी रह जाता?
ज्ञान रुप होकर जीता वह, भक्त मुझे अतिशय भाता ।
आये संयोग-वियोग न अन्तःकरण प्रभावित होता है,
आनन्द-विषाद विकार रहे, वह इनका भार न ढोता है ।
मिल गई परम प्रिय वस्तु जिसे, फिर कहाँ कामना शेष रहे?
फिर कहाँ द्वेष, फिर कहाँ भेद, वह पाप पुण्य से मुक्त रहे।
वह रहा शुभाशुभ परित्यागी, उसमें न ऊगती फलेच्छा,
आसक्ति रहित जो कर्म रहे, उनका प्रारब्ध नहीं बनता ।
निर्वाह हेतु जीवन में जो वह करता कर्म न रहे उसके,
अस्तित्व न अपना शेष रखे, वह आप मुझे धारण करके ।
श्लोक (१८)
हो शत्रु-मित्र जिसको समान, सर्दी-गर्मी में सम रहता,
समभाव रखे सुख-दुख में जो, मानापमान निस्पृह सहता ।
रहता कुसंग से मुक्त सदा, उसके धीरज का पार नहीं,
अप्रभावित लौकिक जीवन से, प्रिय होता मुझको भक्त वही ।
सम रहता शत्रु मित्र में जो, करते न विकल मानापमान,
सुख-दुख, सर्दी-गर्मी जिसको, आते-जाते रहते समान ।
अनुकूल नहीं, प्रतिकूल नहीं, न लगाव रहा अथवा दुराव,
द्वन्द्वों के पार समान रहा, अर्जुन जो जोगी मुक्त भाव ।
इन्द्रिय जित सदा अविचलित जो, सर्वत्र करे भगवददर्शन,
संसर्ग विवर्जित निरासक्त, समभाव धारता जिसका मन ।
काटे या सींचे कोई भी, तरु इसका भेद नहीं करता,
वह योगी प्रिय मुझको अर्जुन, वह वास सदा मुझमें करता ।
न्यायी हो अथवा अन्यायी, दोनों पर मेघ समान झरे,
वह अपना सूर्य उदित करता, अच्छे न बुरे का भेद करे ।
वह सबके साथ समान रहे, आसक्ति नहीं मन में रखता,
अर्जुन वह मेरा भक्त रहा, मेरे गुण उद्घाटित करता
मन्दिर में जले कि कुटिया में, दीपक दोनों को दे प्रकाश,
आकाश रहे समभाव सदा, भावित न करे रितु का विकास ।
समरुप चन्द्रिका सुधा झरे, राजा हो कोई या फकीर,
मेरा प्रिय भक्त रहा अर्जुन, जो योगी ऐसा रहा धीर ।
मन में लवलेश न विषय भाव, केवल मुझमें जो निरत रहा,
समबुद्धि रही, समभाव रहा, सबसे समान व्यवहार रहा ।
उत्तर की हवा कि दक्षिण की, दोनों को मेरु समान लखे,
वह भक्त रहा प्रिय मुझे पार्थ, जो मन के सारे भेद तजे । क्रमशः….