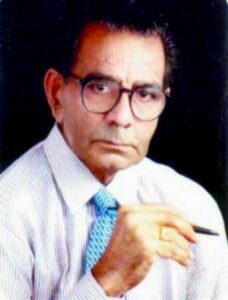 रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।
रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।नवमो ऽध्यायः – ‘राज गुहययोग’
अध्याय नौ – ‘राजविद्या राजमुख्य योग’ सबसे बड़ा ज्ञान/रहस्य, ‘भगवान अपनी सष्टि से बड़ा है’
श्लोक (३)
रहा परम रमणीय आत्मसुख, सुख यह परम पवित्र रहा,
सुखकर रहा समझने में यह, सुलभ और अनुकूल रहा ।
धर्म दृष्टि से सुगम सरलतम, स्वयं प्राप्त होने वाला,
फिर भी जन अज्ञानी इससे विरत रहा आँखों वाला ।
गौ के थन में दूध भरा होता, पर किल्ली उसे तजे,
पीने रक्त अशुद्ध देह की चमड़ी से किल्ली चिपके ।
निकट कमल के भंवरा रहता, मेढ़क भी तो निकट रहे,
पान करे मकरन्द भ्रमर पर मेढ़क कीचड़ में लिपटे ।
द्रव्य गड़ा धरती के भीतर किन्तु मनुज जो अज्ञानी,
रहे दरिद्रावस्था में ही, भोगे नाना दुख प्राणी ।
आत्माराम रहे प्रत्यक्ष सभी के लेकिन अज्ञानी,
भटक वासनाओं में मृगजल में ढूँढा करता पानी
मुँह का अमृत-घूँट बुलक कर, भागे मृग जल के पीछे,
अर्जुन अहंकार का अंधा, उसे न पारस मणि दीखे ।
प्राप्त नहीं वह मुझको होता, गोता खाता रहे सदा,
मैं तो सूरज जैसा खिलकर नित्य सभी के साथ रहा ।
श्रद्धा रहित पुरुष को सम्भव नहीं कि वह मुझको पा ले,
संभव नहीं कि छुटकारा वह, चलती चाकी से पा ले ।
मैं ही अर्जुन मेरु दण्ड बन साधे रखता, काया को,
मुझे समर्पित हुआ न जो, वह लांघ न पाया माया को ।
हे शत्रु विजेता अर्जुन जो, इस भक्ति योग से विमुख रहे,
या श्रद्धाहीन चले पथ पर, वे मुझको नहीं कदापि मिले ।
वे प्राप्त नहीं होते मुझको, बस रहें भटकते उस जग में,
जो मृत्युरुप विकराल रहा, सुख-शान्ति नहीं जिस जीवन में।
श्लोक (४)
मेरी प्राकृत इन्द्रियाँ सजग, इनसे अतीत अव्यक्त रुप,
संपूर्ण जगत में व्याप्त रहा, मेरा वह ही अव्यक्त रुप ।
जड़ चेतन यह ब्रह्माण्ड सकल मुझ में ही सदा अवस्थित है,
पर मैं उनमें हूँ नहीं, पार्थ, यह जग-क्रम पूर्ण व्यवस्थित है ।
मैं निराकार, मैं सगुण पार्थ, अव्यक्त व्यक्त मेरा स्वरुप,
ब्रम्हाण्ड सकल जड़-जंगम जग, धारण करता मेरा स्वरुप ।
परिपूर्ण जगत सारा मुझसे मुझमें ही निहित जगत सारा,
सबसे अतीत, संबंध रहित, अर्जुन यह मेरा पैसारा
परमेश्वर लोकातीत मगर अस्तित्व जगत का उससे है,
लेकिन न रुप कोई ऐसा जो उसे दिखाने सक्षम है ।
परमात्मा को परिपूर्ण रुप से व्यक्त न कोई कर सकता,
वह देशकाल से परे रहा, अभिव्यक्त न होती वास्तविकता ।
अणु अणु में व्याप्त रहा फिर भी संबंध रहित सबसे अतीत,
अपनी महिमा में नित्य सिद्ध, सारा जग हो जाता व्यतीत ।
पा सके पार उसकी महिमा का, ऐसा कोई अन्य नहीं,
सबसे परमेश्वर परे रहा यों विद्यमान वह सभी कहीं ।
मेरा निर्गुण रुप उसी का, सकल विश्व विस्तार रहा,
दूध दही बन जाता जैसे, बीज बिन्दु से तरु उभरा ।
निराकार ही सृष्टि रुप में, ले लेता आकार बड़ा,
मैं ही हूँ आधार, विश्व यह सारा जिस पर रहे सधा ।
महत्तत्व से तन तक सारे भूत-भाव मेरे कारण,
मुझमें भासित रहे, किन्तु मैं उनमें नहीं रहा अर्जुन ।
जैसे जल से फैन बने, पर नहीं फैन में जल रहता,
या संसार बसा सपने में, नींद टूटने पर ढहता । क्रमशः…