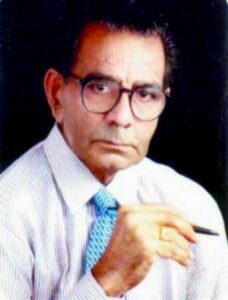 रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।
रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।
सप्तमोऽध्याय – ‘ज्ञान-विज्ञान योग’
श्लोक (२०,२१,२२)
मन हो आए विकृत जिनके बढ़ रहीं लालसायें जिनकी,
गढ़ रहे मूर्तियाँ ईश्वर की, वे फल पाने अपने मन की।
रच रहे विधान अपने, अपने विधियाँ रचते अपनी अपनी,
पाने प्रसन्नता देवों की पूजा करते अपनी अपनी ।
हर भक्त सकाम भावना से भज रहा देव को जो अपने,
श्रद्धा से पूज रहा होता, पूरे करने मन के सपने ।
मैं उसको उसी देवता में श्रद्धा को प्रेरित करता हूँ,
मैं ही हूँ अर्जुन जो उसका, जो पूज्य देवता बनता हूँ।
जिस रूप भाव में श्रद्धा से, भजता है भक्त मुझे अर्जुन,
दृढ़ कर देता हूँ उसी भाव में, भक्ति हेतु भक्तों का मन ।
जो रही भावना भक्तों की, मैं उस जैसा आकार धरै,
करते जो भक्ति सकाम कामना, उनकी सब मैं पूर्ण करूँ ।
जिसका होता जो इष्ट देव, करता जिसका वह आराधन,
फल पाने करता है, पूजन श्रद्धानत करता रहे भजन ।
होती मुराद उसकी पूरी,फल मिलता उसको मनचाहा,
– वह नहीं दूसरे से,अर्जुन, जो फल पाया,मुझसे पाया ।।
श्रद्धा होती है फलीभूत, देवों के रूप रहे मेरे,
मुझको ही पूज रहे होते,विग्रह अनेक रचकर मेरे ।
मैं ही हूँ एक अनेक रूप, रुचि के अनुसार करूँ धारण,
देते हैं फल जो इष्टदेव, देते हैं वे मेरे कारण ।
फलवती कामनाएँ जग की, परितोष क्षणिक दे पाती हैं,
उपजाती नई लालसाएँ, व्याकुल फिर फिर कर जाती हैं।
वे रहे अल्पमति लोग पार्थ, जो पाकर भी कुछ पा न सके,
जिस रूप भजा जिन देवों को, वे उनसे आगे जा न सके ।
हर लिया गया विवेक जिनका, बहु भाँति कामनाओं द्वारा,
भोगों की इच्छा सुखा गई, जिनके सदचिन्तन की धारा ।
अपने स्वभाव से प्रेरित जो, अपने देवों को पूज रहे,
अपना विग्रह गढ़ रहे अलग, सबके न स्वभाव समान रहे ।
वे भक्त जीव जिनकी मति का, कर लिया हरण इच्छाओं ने,
अन्यान्य देव को पूज रहे,आराधन का प्रतिफल पाने ।
जिसका स्वभाव जैसा होता, वैसी उपासना विधि उसकी,
विश्वास रहा जिसका जैसा, वैसी उसकी इच्छा फलती ।
मैं जीव मात्र के अन्तस में, ईश्वर बनकर नित वास करूँ,
इसलिए जीव की हर इच्छा होती है क्या उसको समझें ।
जिस देव रूप के प्रति जैसी श्रद्धा रखता, पूजन करता,
मैं श्रद्धा के अनुरूप उसे उस देव-भक्ति में स्थिर करता ।
श्रद्धापूर्वक आराधन कर, इच्छित भोगों को प्राप्त करे,
उसने यह फल किससे पाया रहता रहस्य, वह क्या समझे?
उसने जो इच्छित फल पाये, मैं ही उनका देने वाला,
उसके देवों की श्रद्धा में, मैं ही होता रहने वाला ।
पहिले से ही निर्धारित है, मेरे द्वारा सबकी क्षमता,
क्षमता से अधिक न दे सकता, कोई भी अधिक न ले सकता।
जो रहे देव सामर्थ्यवान, सब, मेरी आज्ञा पर चलते,
अपनी सीमा में रहते वे, निर्विघ्न कार्य अपने करते ।
श्लोक (२३)
वे अल्पबुद्धि मानुष अर्जुन, जो फल पाने पूजन करते,
सीमित क्षणभंगुर फल होते, जो देवों से उनको मिलते ।
भजते हैं जो जिन देवों को, उनके ही लोक उन्हें मिलते,
मम भक्तों को पर परमधाम, मिलता है, वे मुझमें मिलते ।
जितना सुख भोग भक्त पाता, मधु स्वप्न सरीखा क्षणिक रहा,
जीवन का जितना लाभ मिला, वह जीवन के ही साथ ढला ।
पर भक्ति भावना के कारण, मुझको पा लेते भक्त सभी,
मिलता है मेरा लोक उन्हें, उनका सुख घटता नहीं कभी ।
जो भजे देवताओं को वे, पाते है देवलोक मरकर,
पाते हैं मेरा परमलोक जो, भक्त रहे मुझसे जुड़कर ।
लोकोत्तर ब्रह्म रूप मुझको, जानें सब सम्भव नहीं रहा,
इसलिए विविध रूपों की लेकर, शरण भक्त ने मुझे भजा ।
जिस तल तक भक्त पहुँच जाता उस तल का सुख वह पा जाए,
अनुभूति गहनतम हुई कि उसको अन्तिम तल भी मिल जाए।
तल वह अस्तित्व अखण्ड अमित, जो परम रहा, सम्पूर्ण रहा,
हर अर्थवान हो अर्थ हीन, जिसके आगे निर्मूल्य रहा ।
श्लोक (२४,२५)
मुझको न जानने वाले वे, मतिहीन मनुज यह समझ रहे,
व्यक्तित्व रूप यह मेरा है, आराधक जिसको विरच रहे ।
यह अल्पज्ञान ही है उनका, वे मुझे नहीं पहिचान सके,
उत्तम अविनाशी मम स्वरूप,उर में न इसे वे धार सके ।
अल्पज्ञ मूढ़ जन के आगे, मैं प्रकट न होता कभी पार्थ,
नित रखूँ छिपाकर माया में, उन लोगों से अपना यथार्थ ।
माया मोहित यह जगत अस्तु जाने न अजन्मा अच्युत को,
नित अविनाशी जिसका स्वरूप उस परा तत्त्व को या मुझको ।
मैं परमाधार प्रकृतियों का, यह नहीं समझते बुद्धिहीन,
मुझसे उत्तम कोई न रहा, यह नहीं समझते बुद्धिहीन ।
गोतीत अचिन्त्य में अविनाशी, वे व्यक्त मुझे समझा करते,
जो पराभाव मेरा अर्जुन, उसको मति मन्द नहीं लखते ।
प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ मैं, ढक रखती मुझे योग माया,
होती है प्रकट जगत में जो, वह होती है मेरी छाया ।
अज्ञानी मुझे न जान सकें, मुझको अपने जैसा समझें,
लेता हूँ जन्म मरण पाता, ऐसा अविनाशी को समझे ।
मैं निरावरण, मुझसे न अलग, कान्तय, योग माया मेरी,
यह रहा दृष्टियों पर पर्दा, रचती जिसको माया मेरी ।
सूरज न दीखता नेत्रों को, जब घिर आते बादल काले
सूरज तो सूरज रहे सदा, हमने पट नेत्रों पर डाले
यह रहा आवरण काया का, जो हमको अन्धा किए हुए,
मदमते रहे हम दृष्टि हीन, जो देहबुद्धि के साथ जिए ।
उसको न देख पाए जग में, जो शुद्ध प्रकाश रूप छाया,
क्या पानी रसविहीन कोई, वह कौन? जगत जिसकी माया ।
वे व्यक्त हुआ समझे मुझको, मेरा स्वभाव अव्यक्त रहा,
मुझमें न हुआ कुछ परिवर्तन, मैं तो सर्वत्र समान रहा ।
मुझ रूपहीन पर तरह तरह, के रूपों का कर आरोपण,
सम्पुष्ट कर चलें अपना मन, करके मेरा झूठा चिन्तन ।
सब देवों में बस जाता, पर परमात्मा केवल एक रहा,
वह कभी विभाजित हुआ नहीं, वह बटा, परन्तु अखण्ड रहा ।
सब रूपों में रह विद्यमान, वह सबसे परे परात्पर है,
वह केन्द्र अचल सारी गति का, वह अन्तहीनता का बल है।
यह जगत मूढ क्या जानेगा, जो सृजनशीलता है मेरी
मोहित करके जग को रखती, वह रही योगमाया मेरी
सम्मुख न किसी के आता मैं,वह बनी आवरण रहती है
वह मुझे जगाए रखती है,वह मुझे सुलाए रखती है।क्रमशः…