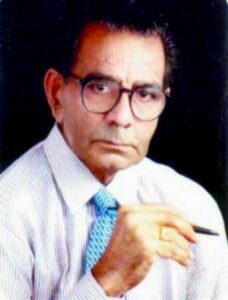 रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।
रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।
सप्तमोऽध्याय – ‘ज्ञान-विज्ञान योग’
श्लोक (६)
जड़-चेतन जो भी जग में, है परिणाम प्रकृतियों का मेरी,
उत्पन्न परा- अपरा से, है अस्तित्व छाप बनता मेरी ।
इसलिए सत्य यह है अर्जुन, उत्पत्ति जगत की है मुझसे,
मैं प्रलय करूँ विलयन जग का, लय, विलय सभी जग का मुझसे ।
इसलिए धनञ्जय अन्य तत्त्व, कोई भी श्रेष्ठ नहीं मुझसे,
सब अनुस्यूत मणिमाला के, मानो बनकर रहते मनके ।
जिसकी मैं ही रचना करता, मैं ही करता जिसको धारण,
मेरे आश्रित सब कार्य रहे, मैं ही सब कार्यों का कारण
सम्पूर्ण जगत यह गुथा हुआ,मुझ एक सूत की माला में,
मुझसे न भिन्न कारण कोई,हूँ परमाधार निराला मैं ।
मैं सर्वरूप में सर्वव्याप्त, मुझमें ही सारा विश्व बसा,
मैं रहा प्रभव मैं रहा प्रलय, मैंने ही सारा विश्व रचा ।
जब सूक्ष्म प्रकृति स्थूल, प्रकृति से, करे मेल-जग जगता है,
टकसाल काम करती मानो, सिक्के का जीवन ढलता है ।
संयोजित होते पंचतत्व,पर कोटि जातियाँ रहें भिन्न,
पहिचान चेतना की सबमें, बसती लेकिन होकर अनन्य ।
अव्यक्त कहें या माया का,भाण्डार अपरिमित भर जाता,
माया के द्वारा सिक्के की, कीमत का चिन्ह उभर आता ।
माया से ही निर्मित सिक्का, माया में ही व्यवहार करे,
घिस पिट जाए हो मूल्य हीन, पड़कर भट्टी में पुनः गले ।
इन नामरूप जग जीवों का, विस्तार प्रकृति ही करती है,
लगती है मिथ्या किन्तु प्रकृति, यह जुड़ी पुरुष से चलती है ।
अर्जुन यह अन्तर्वाहय विश्व, मानो ऐसी मणिमाल रही,
मेरे ही तागे में मेरी ही मणियों की, ज्यों गुथी लड़ी ।
मणिमाला का मैं तार रहा, मैं ही मणिमाला का मनका,
मैं ही उसकी रचना करता, मैं ही उसको धारण करता ।
मणिमाला की शोभा लखता, मैं ही अव्यक्त करूँ विचरण,
मैं हर मनके का प्राण रहा, यह मणिमाला मेरा प्रगटन ।
यह प्रकृति निम्नतर है, मेरी यह प्रकृति उच्चतर मेरी है,
जड़ जंगम दोनों रूपों में,जिसने यह सृष्टि सहेजी है ।
‘क्षेत्रज्ञ रहा चेतन जिसमें जो रहा अचेतन ‘क्षेत्र वही,
है ‘परा’ उच्चतर प्रकृति, निम्न जो ‘अपरा’ है वह कही गई।
सम्पूर्ण अचेतना की द्योतक, यह प्रकृति, इसे समझो अर्जुन,
सम्पूर्ण चेतना का तल भी, इसमें संन्निहित रहा अर्जुन ।
आत्मा, शरीर ये दो पहलू क्षेत्रज्ञ’ क्षेत्र’ दो किन्तु एक,
बनती मिटती रहती है इनके बीच उभरती एक रेख ।
है कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो मुझसे कहीं उच्चतर हो,
है कोई ऐसा कार्य नहीं, जो मुझे कभी भी दुष्कर हो ।
जग की सारी सत्ताओं को, मैं रखूँ नियन्त्रित एक साथ,
मैं सभी कारणों का कारण, मुझसे जीवन मुझसे विनाश । क्रमश …