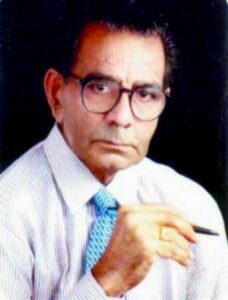 रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।
रचित ‘गीताज्ञानप्रभा’ ग्रंथ एक अमूल्य ,धार्मिक साहित्यिक धरोहर है, जिसमे डॉक्टर साहब द्वारा ज्ञानेश्वरीजी महाराज रचित ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद किया है, श्रीमद्भगवतगीता के 700 संस्कृत श्लोकों को गीता ज्ञान प्रभा में 2868 विलक्ष्ण छंदों में समेटा गया है।अष्टमोऽध्यायः – ‘अक्षर ब्रह्मयोग’
अध्याय आठ – ‘भगवतप्राप्ति योग’ या विश्व के विकास का क्रम और भगवत प्राप्ति “
श्लोक (१२,१३)
पालन कर योग-धारणा तू, इन्द्रिय द्वारों का कर निरोध,
अन्तर्यामी परमात्मा में, मन संस्थापित कर निर्विरोध ।
मस्तक में ऊर्ध्वारोहण से, संस्थापित कर तू प्राण वायु,
ध्यानस्थ योग में मेरे हो, हे पार्थ प्राप्त कर तू चिरायु ।
इस योग-धारणा में बसकर, जो अक्षर ब्रम्ह को पहिचाने,
उच्चारित पावन मन्त्र करे, जो ब्रम्ह रुप मुझको माने ।
इस तरह ध्यान मेरा करता, तजता है जो शरीर अर्जुन,
मिलता है भगवद् धाम उसे, सार्थक होता उसका जीवन ।
कर ले दस द्वार बन्द अपने, कर अन्तर्मुखी वृत्ति अपनी,
हृदयेश वहाँ मन सुस्थिर कर, संयत मति गति कर ले अपनी ।
मन के द्वारा प्राणों को तू, अपने मस्तक में धारण कर,
ओंकार ब्रह्म जो परम पुरुष, होकर विभोर उच्चारण कर
बन जाता है आज्ञाकारी, योगी का क्रमशः साधन से,
होता है प्राणायाम सफल ओंकार प्रणव के धारण से ।
जिस तरह अपंग हुआ प्राणी, हलचल न अधिक कर पता है,
मन उसी तरह ओंकार ध्यान से, लुंज पुंज हो जाता है ।
ओंकार ब्रम्ह का अर्थरुप, मुझ निर्गुण का चिन्तन करता,
जो योगी तजता है शरीर, वह पुरुष परम गति को वरता ।
मन प्राणों के ही साथ-साथ, मस्तक में अविचल बस जाता,
इस योग-धारणा में, साधक मन की निश्चलता को पाता
जो निराकार निर्गुण उसको, साधन से साधक पाता है,
वह निराकार के सगुण भाव से पहिले परिचय लाता है।
अभ्यास योग का है जिसको, वह साध सके मन को अपने,
उसको भी, नित्य निरंतर मन जिसका लगता प्रभु को जपने ।
हृदयस्थ आत्मा नाड़ी से होकर जब ब्रह्मरन्ध्र पहुँचे,
वह छोर सुषुम्ना का होता, उससे वह फिर बाहर निकले ।
तब परमात्मा के साथ मेल उसका होता, तद्गत होता,
जो रहा उच्चतम लक्ष्य उसे, तजकर शरीर, योगी वरता ।
जो प्रणव ‘ॐ’ है ब्रम्ह स्वयं, जिसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं,
जो निराकार-निर्गुण होकर भी व्याप रहा है सभी कहीं ।
उसका ही ध्यान किया जाता, लयमान उसी में होने तक,
जो ब्रह्मानंद स्वरुप उसी में प्राणवायु के खोने तक
श्लोक (१४,१५)
तुम सोच रहे होंगे अर्जुन, जब समय मृत्यु का आयेगा,
होगा वह कौन कि उस क्षण जो इन्द्रिय का संयम साधेगा?
जीवन के सुख हो रहे नष्ट अरु रहीं इन्द्रियाँ संकट में,
ओंकार नाम तब आयेगा क्या उभर सहज ही अन्तर में?
मत ऐसा संशय व्यर्थ करो, जो मेरी सेवा करता है,
अर्जुन अपने अन्तिम क्षण में, वह मुझको नहीं बिरसता है।
मैं भी रखता हूँ ध्यान सदा, अपने सेवक का भली भांति,
जो मुझे हृदय में बसा रखें, उसकी हट जाती है विभ्रान्ति ।
उनको न क्षुधा फिर सता सके, उनके वश में होती इच्छा,
विषयों की रे आसक्ति कहाँ? मन उनका मुझमें रहे रमा ।
जो होते मेरे भक्त उन्हें मैं स्वयं उबारा करता हूँ,
वे मुझे पुकारा करते हैं, मैं दौड़ा जाया करता हूँ।
उनको न ग्लानि होने पाए, इसलिए प्रबोधित करता हूँ,
तन के पिंजरे में रहे मगर मैं उन्हें सुलभ नभ करता हूँ।
भक्तों को निज तन तजने का, रंचक भी शोक नहीं होता,
तन तजकर मेरा भक्त सदा, मेरे स्वरुप में लय होता ।
वह तन से बिछुड़ रहा ऐसा, रखता है मन में भाव नहीं,
उसका है मुझसे प्रेम, देह से है उसको अनुराग नहीं ।
वह मुझसे मिलने के सुख में, सारी बाधाएँ भूल रहे,
मेरा ही केवल मेरा ही, आत्मा में उसकी, तेज जगे ।
मैं सदा निकट रहता उसके, उसकी श्वासा में बसता हूँ,
वह मुझे समर्पित रहता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ।
वह शुद्ध हृदय से जब टेरे, मैं दौड़ पड़ें सुनकर पुकार,
जो ध्यान करें मेरा उनके, अन्तस में करता मैं निवास ।
मुझमें अनन्य चित होकर जो नित ध्यान किया करता मेरा,
उस नित्य निरंतर योगी को होता है सुलभ साथ मेरा ।
मेरा वियोग यह सके नहीं, वह भक्त मुझे तत्क्षण पाता,
हे पार्थ वियोग असह मुझको, अपने भक्तों का हो जाता ।
अतिशय श्रद्धा अरु प्रेम सघन, जब भजन ध्यान को सिद्ध करें,
वे सिद्ध महात्मा पार्थ मुझे, अपने जीवन में प्राप्त करें ।
उनका न दुबारा जन्म हुआ, वे तो बस मुझको प्राप्त हुए,
कर्मो के पाश नष्ट होते, मुझसे मिल वे मद्रुप हुए ।
मुझ तक जो आत्माएँ पहुंची, फिर जन्म न उनका हुआ कभी,
पा लेती है वे परम-सिद्धि, धारण करतीं फिर देह नहीं ।
वह देह रही जो दुख का घर, जो क्षण भंगुर जो है अनित्य,
जो रही व्याधियों का कारण, जो मिथ्या सुख में रही लिप्त ।
तन दुख तरुओं का है अरण्य, गुरसी यह तीनों तापों की,
मानव-तन उस बलि के समान जो मरण-काक को दी जाती ।
दारिद्रय बढ़ाने वाला यह, भय से कंपित करने वाला,
भाण्डार दुखों का, कष्टों का, संशय से मन भरने वाला।
यह करने वाला बुद्धि भ्रष्ट, फल पूर्व जन्म के कृत्यों का
आधार जगत जंजालों का कण्टक वन अहम विकारों का।
यह थाल परोसा हुआ जहाँ होते व्यंजन बीमारी के
जिसमें कृतान्त की जूठन है, उपक्रम सब मारामारी के ।
आशा की जलती झोपड़िया, खल जन्म मरण का भ्रान्ति भरा,
यह रहा बाघ की गुफा, मोह का जाल मरुस्थल दाह भरा।
शीतलता का विष घूंट रहा, विश्वास कि जो छलता रहता,
दुश्मन का आदिराथित्य रहा वह चक्र कि जो दलता रहता ।
सागर यह सभी अनर्थों का, सुन्दर पर विष की बेल रही,
लहरों से टूट बिखर जाये, यह ऐसी जर्जर रही तरी ।
मृगजल से सींचा हुआ विपिन, आकाश धुएँ से भरा हुआ,
ऐसा शरीर फिर नहीं मिला, योगी का जो मद्रुप हुआ ।
हे अर्जुन भाव अनन्य लिए, जो नित्य निरंतर भजे मुझे,
उसका हित मैं देखा करता, मैं रहूँ सहज उपलब्ध उसे ।
संलग्न भक्ति में वह मेरी, अन्यान्य ध्यान कुछ भी न रखे,
उस निरासक्त में मुक्ति हेतु, बाकी कोई इच्छा न बचे ।
पा लिया मुझे जिन भक्तों ने फिर उनका जन्म नहीं होता,
वे रहे महात्मा योगी जन उनका उद्धार स्वंय होता ।
जग यह अनित्य दुख दाह भरा उनको न प्रभावित कर पाये,
संसिद्धि प्राप्त कर भक्त स्वंय भारित प्रभुता से हो जाये। क्रमशः…